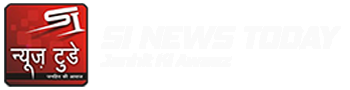Know what the difference is in the Representation of the People Act 1950 and the Representation of the People Act, 1951
#DoYouKnow #IndianConstitution #IndianLaw #ECI #BritishLaw #RepresentationofthePeopleAct #Humara_Janpratinidhi #हमारा_जनप्रतिनिधि #IndependenceDay2018 #Nationalism
भारत प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र भारत के संविधान की कभी दूर न होने वाली बुनियादी विशेषताओं में से एक है तथा यह इसकी बुनियादी संरचना का अंग है। लोकतंत्र की परिकल्पना (जैसे कि संविधान में परिकल्पित की गई है) चुनाव की विध से संसद और राज्य विधायिकाओं में जनप्रतिनिधित्व की पूर्व कल्पना करती है। लोेकतंत्र के बने रहने के लिए कानून के शासन को बने रहना चाहिए तथा यह आवश्यक है कि बेहतरीन उपलब्ध व्यक्ति देश के समुचित शासन के लिए जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने चाहिए। और जन प्रतिनिधि के रूप में बेहतरीन उपलब्ध व्यक्तियों के चुने जाने के लिए चुनाव ऐसे वातावरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाने चाहिए जहां निर्वाचक अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार अपने वोट का इस्तेमाल करने में समर्थ हों। इस प्रकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ का निर्माण करते हैं।
भारत ने सरकार बनाने के लिए ब्रिटिश संसदीय प्रणाली अपनाई है। हमारे यहां निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित उपराष्ट्रपति, निर्वाचित संसद और हर राज्य के लिए निर्वाचित राज्य विधायिकाएं हैं। अब हमारे यहां निर्वाचित नगरपालिकाएं, पंचायतें और अन्य स्थानीय निकाय भी हैं। इन कार्यालयों और निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तीन पूर्वापेक्षाएं हैं – 1. इन चुनावों को कराने के लिए एक प्राधिकरण जो राजनीतिक एवं कार्यकारी हस्तक्षेप से अलग होना चाहिए, 2. कानून जो चुनाव कराने को शासित करें और उस प्राधिकरण के अनुरूप हों जिसे इन चुनावों को कराने के जिम्मेदारी दी गई हो तथा 3. एक व्यवस्था जहां इन चुनावों के संबंध में उत्पन्न सभी संदेह और विवाद निपटाए जाने चाहिएं।
भारत के संवधिान में इन सभी अनिवार्यताओं पर उचित ध्यान दिया गया है तथा सभी तीनों मामलों के लिए उचित रूप से उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव कराना दो कानूनों के प्रावधानों से शासित होता है – जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951।
#Humara_Janpratinidhi #हमारा_जनप्रतिनिधि जिस तरह से देश में यूपीएससी, डिफेंस सर्विसेज, एयर फोर्स, इंडियन नेवी पदों के लिए किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए. ठीक उसी तरह क्या पार्लियामेंट में बैठने वाले दबंग नेताओं के लिए कोई नियम कानून होने चाहिए?
— SI News Today (@sinewstoday) August 12, 2018
1. जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 मुख्य रूप से निर्वाचक सूचियों की तैयारी और संशोधन संबंधी मामलों से संबंधित है। इस कानून के प्रावधानों के पूरक के रूप में इस कानून की धारा 28 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 बनाए हैं तथा ये नियम निर्वाचक सूचियों की तैयारी, उनके आवधिक संशोधन और अद्यतन, पात्र नाम शामिल करने, कुपात्र नाम हटाने, विवरण इत्यादि ठीक करने संबंधी सभी पहलुओं को देखते हैं। ये नियम राज्य की लागत पर फोटो सहित पंजीकृत मतदाताओं के पहचान कार्ड के मुद्दे भी देखते हैं। ये नियम अन्य विवरण के अलावा निर्वाचक के फोटो सहित फोटो निर्वाचक सूचियां तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त भी बनाते हैं।
2. चुनावों का वास्तविक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों से शासित हैं जो इस कानून की धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 से पूरित किए गए हैं। चुनाव के संबंध में या उससे उत्पन्न सभी संदेह और विवाद से जुड़े चुनाव बाद के सभी मामलों का निपटारा भी जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। इस कानून के तहत ऐसे सभी संदेह और विवाद संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए जा सकते हैं लेकिन सिर्फ चुनाव होने के बाद ही ऐसा किया जा सकता है तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता।
उक्त उल्लेखित जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 तथा निर्वाचकों के पंजीकरण्र नियम 1960 तथा चुनाव आयोजन नियम 1961 पूर्ण संहिता का निर्माण करते है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य विधायिकाओं के चुनाव संबंधी सभी मामले देखता है। निर्वाचन आयोग या उसके तहत काम करने वाले किसी प्राधिकार के किसी निर्णय से असंतुष्ट कोई व्यक्ति इन कानूनों और नियमों के अनुरूप राहत पा सकता है।
Source- भारत के निर्वाचक कानून